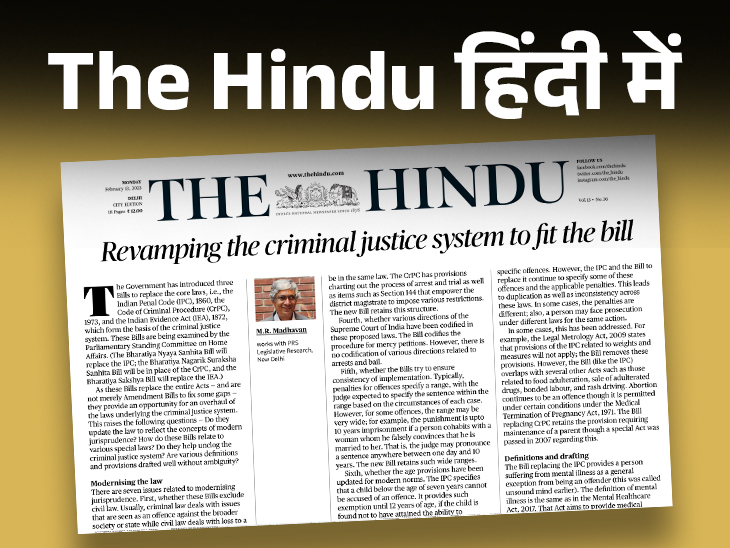
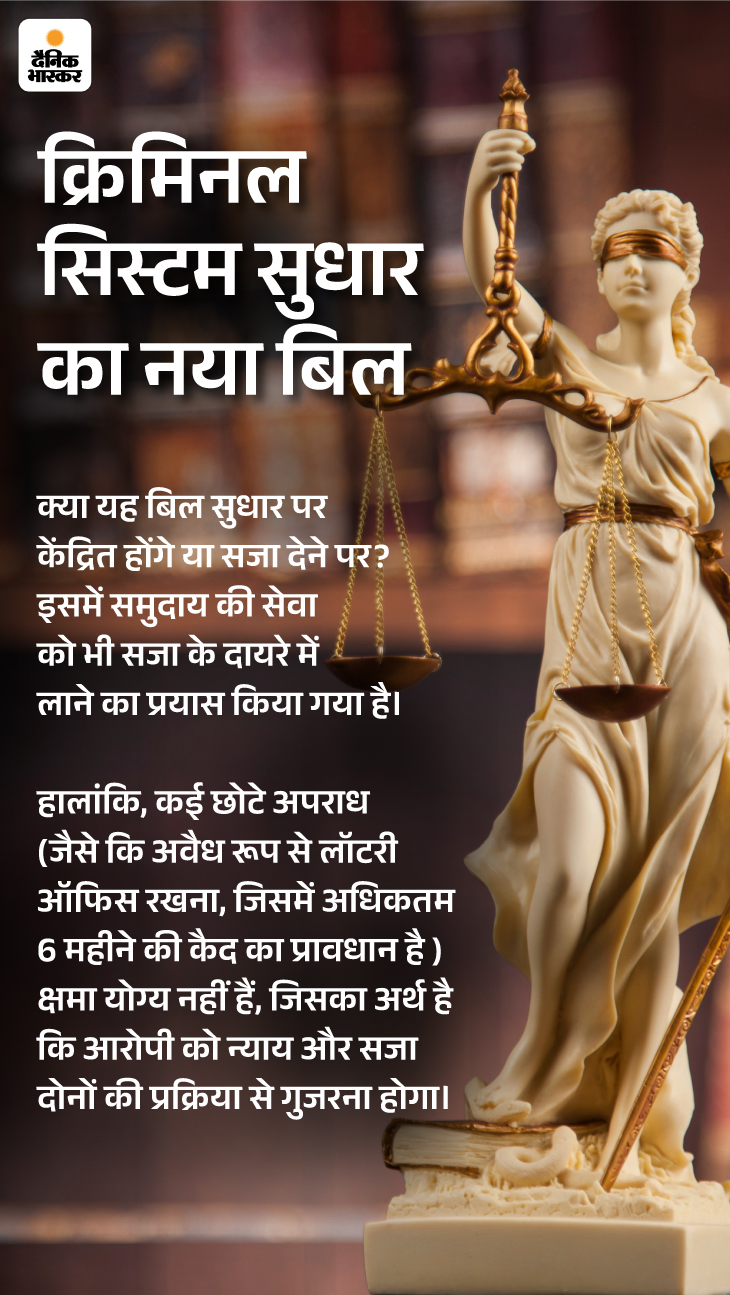
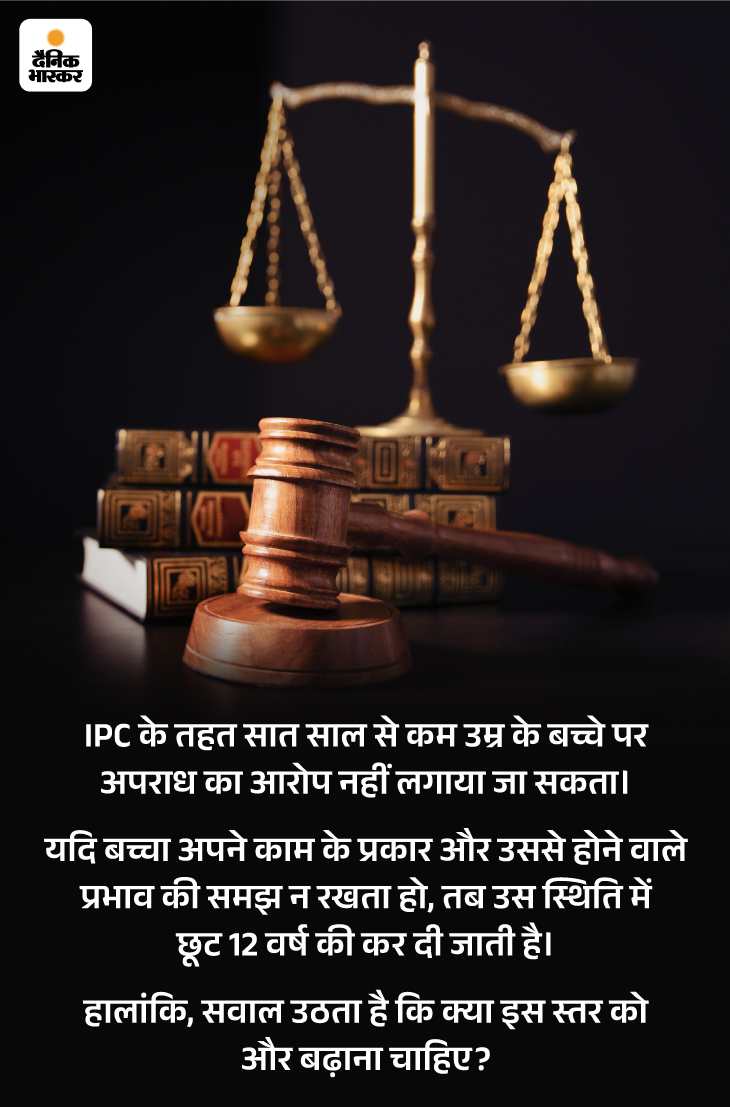
- Hindi News
- Career
- What Is The New Bill To Reform The Criminal Justice System? Read The Editorial Of November 11
13 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
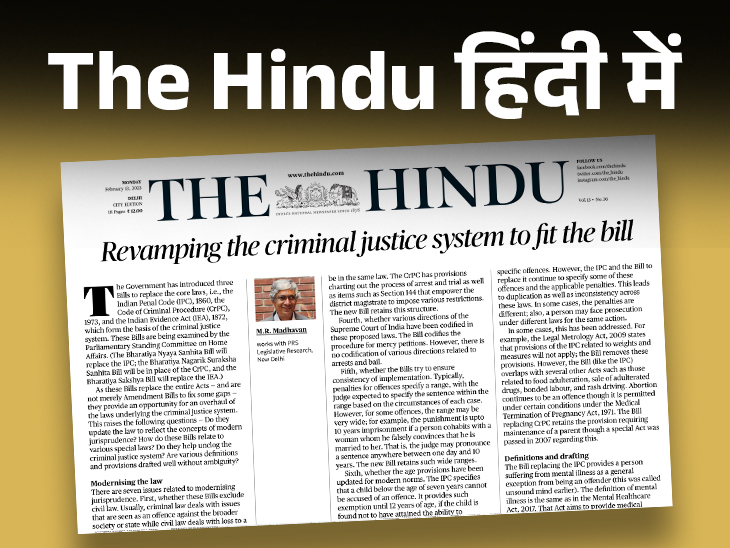
भारत सरकार ने बुनियादी कानूनों में बदलाव के लिए तीन बिल प्रस्तुत किए हैं; इंडियन पीनल कोड ( IPC ), 1860, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ( CrPC), 1973, और इंडियन एविडेंस एक्ट ( IEA ), 1872।
यह तीनों कानून क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आधार हैं। इन सभी बिल की जांच होम अफेयर्स की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कर रही है।
IPC की जगह, भारतीय न्याय संहिता बिल, CrPC की जगह, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल और IEA की जगह भारतीय साक्ष्य बिल लाया जाएगा।
चूंकि यह बिल सिर्फ संशोधन बिल नहीं है, जो कुछ समस्याओं के समाधान के लिए लागू किया जाए , बल्कि ये बिल पूरे कानून को बदल देंगे। ये बिल मौजूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बुनियादी बदलाव करने का मौका देते हैं।
इससे यह सवाल भी उठते हैं, क्या यह बदलाव आधुनिक न्याय विज्ञान के विचार को ध्यान में रख कर किये गए हैं? यह बिल विभिन्न विशेष कानूनों से कैसे संबंधित हैं?
क्या यह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बाधाओं को दूर करेंगे? क्या तमाम परिभाषाएं और प्रावधान इस तरह से तैयार किए गए हैं कि उनमें कोई अनिश्चितता ना हो?
कानूनों का आधुनिकीकरण
न्याय विज्ञान के आधुनिकीकरण से संबंधित सात समस्याएं हैं।
पहला, क्या ये बिल सिविल लॉ को बाहर रखता है? आमतौर पर क्रिमिनल कानून ऐसे मामलों पर ध्यान देते हैं, जहां अपराध समाज के एक बड़े हिस्से या राज्य के प्रति किया गया हो, जबकि सिविल कानून में ये किसी व्यक्ति के नुकसान से जुड़े मामले पर लागू होते हैं।
हालांकि, CrPC में तलाक के बाद महिला और बच्चे को सहारा देने संबंधी प्रावधान हैं। हालांकि ये कानून इजाजत देता है कि धोखाधड़ी के शिकार व्यक्ति को पैसे देकर अपराधी अपने आप को बरी करवा सके।
जैसे कि धोखाधड़ी का शिकार व्यक्ति, कई मामलों में खुद ही आरोपी को माफ कर सकता है। सवाल यह है कि क्या ऐसे मामले भी सिविल कोड में शामिल होंगे? क्या नए बिल में ऐसे प्रावधान बनाए रखे गए हैं?
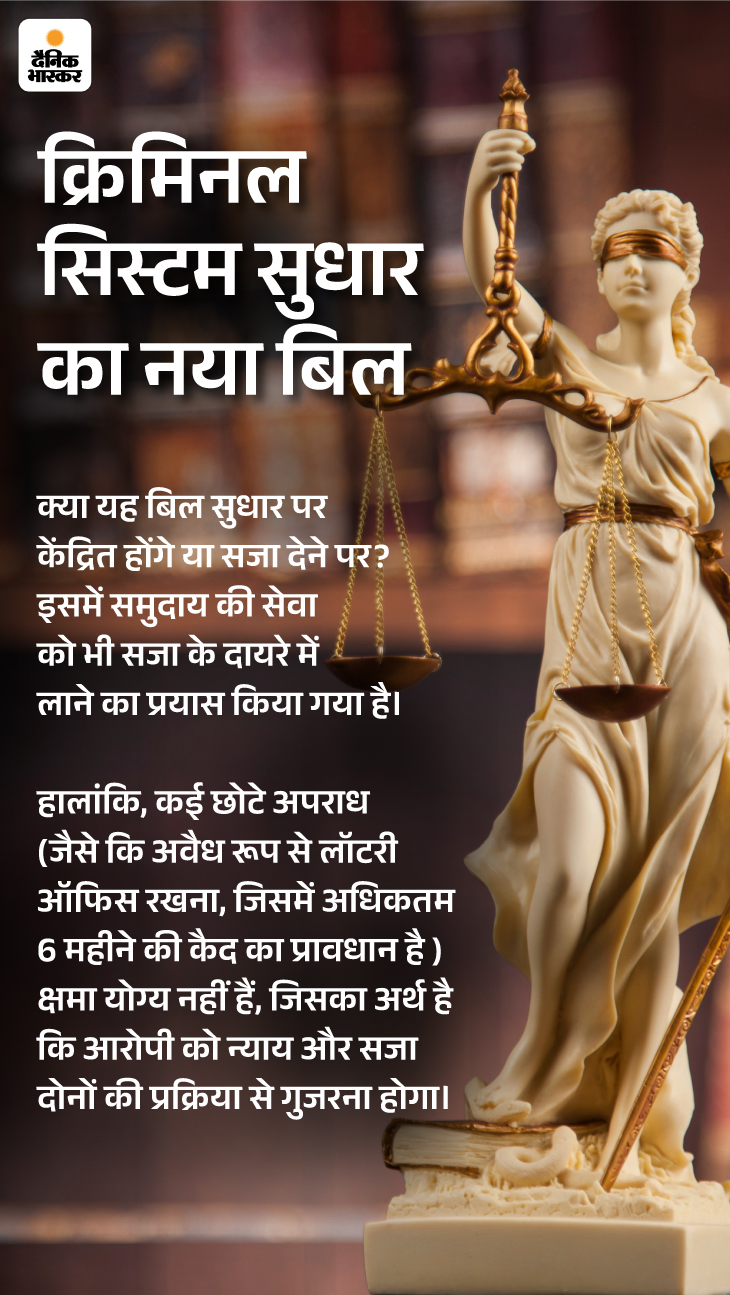
तीसरा, क्या लोगों की न्याय व्यवस्था और क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन एक ही कानून के तहत आने चाहिए? CrPC में गिरफ्तारी और न्याय प्रक्रिया से संबंधित निर्देश हैं।
जैसे की धारा 144 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को विभिन्न तरह की रोक लगाने का अधिकार है। क्या नए बिल में ऐसे ढांचे को सुरक्षित रखा गया है?
चौथा, क्या सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देश इन प्रस्तावित कानून में शामिल किए गए हैं? यह बिल दया याचिका को संहिता में लिखित रूप से सुनिश्चित करता है। हालांकि, इसमें गिरफ्तारी और जमानत से जुड़े निर्देश साफ तौर पर नहीं बताए गए हैं।
पांचवा, क्या यह बिल समान रूप से लागू किया जा सकता? आमतौर पर अपराधों की सजा में एक सीमा तय की जाती है।
जज से यह उम्मीद रखी जाती है कि वह सजा देने में हालात को देखते हुए इस समय सीमा का ख्याल रखेंगे। हालांकि, कुछ अपराधों में यह सीमा बहुत लंबी हो सकती है।
जैसे, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को झूठे विवाह का यकीन दिलाकर अपने साथ रखता है, उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है।
इसका अर्थ है कि जज उस व्यक्ति को एक दिन से लेकर 10 साल तक की सजा सुना सकते हैं। नए बिल में इस तरह की लंबी समय सीमा को बदला नहीं किया है।
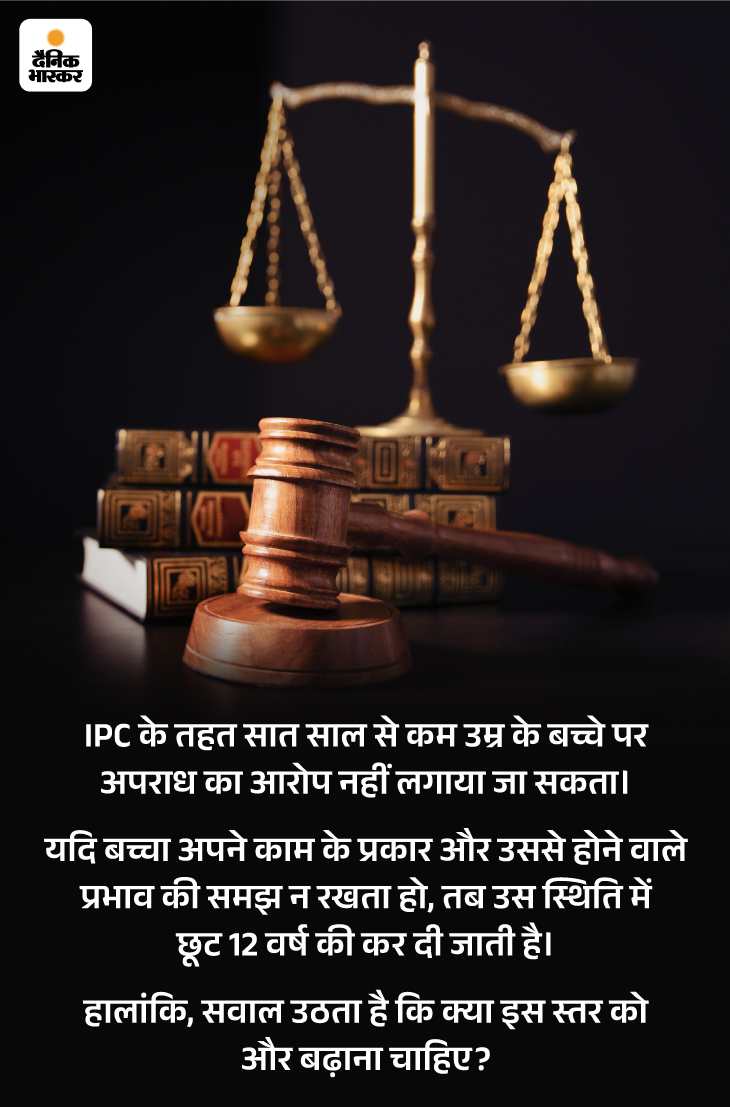
सातवां, क्या जेंडर संबंधी अपराध में बदलाव किया गया है? यह बिल सुप्रीम कोर्ट में समान जेंडर के संबंध को गैरकानूनी बनाए रखने के फैसले से सहमति दर्शाता है।
IPC की धारा 377, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया था, उसे इसमें छोड़ दिया गया है।
इस धारा के तहत यदि एक ही जेंडर के दो वयस्कों द्वारा सहमति से संबंध बनाया जाता है, तो वह अपराध नहीं माना जाता।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में पुरुषों के रेप और वहशीपन से संबंधित लिखी बातों को भी हटा दिया गया है।
2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी की वैवाहिक रेप को अपराध मानने की सिफारिश में भी कोई बदलाव नहीं किया गया।
कुछ विशेष कानूनों का दोहराया जाना
IPC को 1860 में अपराध और सजा के मुख्य कानून के रूप में लागू किया गया था। उसके बाद, अब तक खास अपराधों के लिए कई कानून बनाए और लागू किये गए हैं।
हालांकि, IPC और उसके जगह पर लाया जाने वाला बिल, कुछ अपराधों और उनकी सजा को परिभाषित करता है।
इस वजह से कई कानून दोहराए गए हैं, जिससे इसमें कानून पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ मामलों में अलग-अलग सजा तय की गई हैं, जिससे एक ही व्यक्ति एक अपराध के लिए विभिन्न न्याय प्रक्रिया से गुजरेगा।
कुछ मामलों में इसमें सुधार भी किया गया है। जैसे कि ‘द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009’ में कहा गया है कि IPC के प्रावधान नाप तोल संबंधित मामलों पर लागू नहीं होंगे, इस बिल में उन प्रावधानों को हटा दिया गया है।
हालांकि, इस बिल में ( IPC की तरह ) खाने में मिलावट, नकली दवा बेचने, बंधुआ मजदूरी और बुरे तरीके से गाड़ी चलाने के लिए कानून लाए गए हैं, जिन पर पहले से ही कई अन्य कानून लागू हैं।
इसमें अबॉर्शन अभी भी एक अपराध है, जबकि विशेष परिस्थितियों में इसकी इजाजत मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971 के तहत दी जाती है।
CrPC की जगह आने वाले बिल में माता-पिता द्वारा देखभाल की जरूरत हो बनाए रखा गया है। यह विशेष एक्ट 2007 में लाया गया था।
परिभाषाएं और प्रारूप बनाने की प्रक्रिया
IPC के जगह आने वाले बिल में मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति को आम तौर पर अपराधी नहीं माना जाएगा ( पहले के कानूनों में ऐसे लोगों को बददिमाग कहा जाता था।
मानसिक बीमारी की परिभाषा मेडिकल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 से ली गई है। इस एक्ट द्वारा मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को इलाज देने की कोशिश की गई है, इसलिए इससे मंद बुद्धि और अधूरे मानसिक विकास को बाहर रखा गया है।
जबकि शराब और ड्रग्स की आदत को भी इसमें शामिल किया गया है, यानी अब नए बिल में उस व्यक्ति को छूट दी गई है, जो शराब और ड्रग्स के नशे का आदी है, लेकिन उन्हें नहीं, जो मानसिक विकास न हो पाने के कारण अपने कामों के दुष्प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं।
इन तीनों कानून में आम जीवन से कई उदाहरण दिए गए हैं, ताकि प्रावधानों को सही तरह से समझाया जा सके। हालांकि, इनमें से कुछ उदाहरण पुराने हो गए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें शामिल किया गया है।
जैसे की रथ की सवारी, तोप के गोले दागना और पालकी की सवारी। बेहतर होगा कि इन उदाहरण की जगह आधुनिक जीवन के घटनाओं को शामिल किया जाए।
यह सभी बिल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आधार होंगे, इसलिए संसद को इनकी जांच बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए, ताकि वह एक निष्पक्ष, न्यायोचित और बेहतर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन सके।
IPC, CrPC और IEA की जगह लाए जा रहे, नए बिल संसद द्वारा सावधानी से जांच किए जाने चाहिए, ताकि निष्पक्ष, न्यायोचित और योग्य क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाया जा सके।
लेखक: एम. आर. माधवन, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, न्यू दिल्ली के साथ कार्यरत हैं
Source: The Hindu
[ad_2]
Source link


